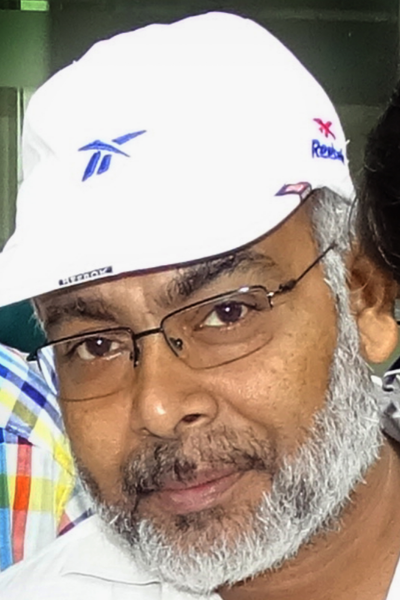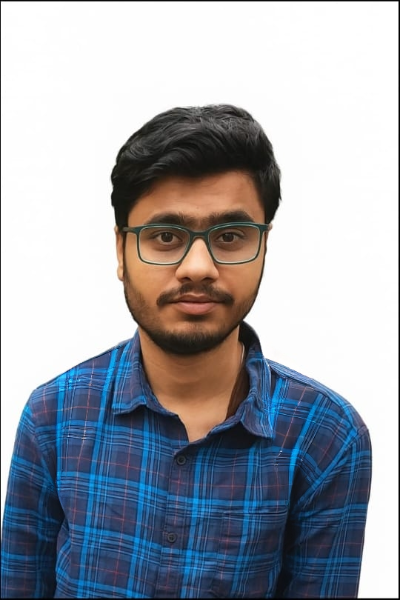ए. जे. सी. बोस भारतीय वानस्पतिक उद्यान
किसी भी वानस्पतिक उद्यान को असंख्य पौधों के संग्रहों का एक खुला संग्रहालय कहा जा सकता है जहाँ वृक्षों, झाड़ियों, बूटियों, लत्तों, कठबेलों आदि को वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित, अंतर्राष्ट्रीय रूप में मान्य वर्गीकरण के आधार पर समुचित रूप से लेबल किया जाता है, एवं जातियों की अच्छी समझ के लिए सन्निकट संबंधित समूहों/पौधों को विशेषकर साथ में उगाए जाते हैं | वानस्पतिक उद्यान में वृक्ष एक विशेष भाग में होते हैं जिसे आर्बोरेटम कहा जाता है; चीड़ के वृक्षों सहित जिम्नोस्पर्मस को पाइनेटम में व्यवस्थित किया जाता है; स्क्रिवपाइन्स यानि पेंडेनस पेंडेनेटम में उगाए जाते हैं; ऑर्किड्स को ऑर्कीर्डियम में सम्मिलित किया जाता है; बांसों का पोषण बम्बूसेटम में किया जाता है एवं पामों को पामेटम में संरक्षित किया जाता है |
अलमॉन्ड के अनुसार (1993),वानस्पतिक उद्यान सतत परिवर्तन होने वाली जीवंत पौधों का संग्रहालय है | चक्रवर्ति एवं मुखोपाध्याय (1990) ने वानस्पतिक उद्यान को पौधों का जीवंत भंडारगृह या आश्रयस्थल के रूप में वर्णन किया है जहाँ वैज्ञानिक आधार पर पौधों को व्यवस्थित एवं रख-रखाव किया जाता है और जहाँ पहचान हेतु संग्रहों को सामान्यतः लेबल एवं चिन्हित किया जाता है | हेवुड (1983 ) का मत है की वानस्पतिक उद्यान एवं आर्बोरेटम दुर्लभ एवं लुप्तप्राय जातियों के संरक्षण एवं रख-रखाव के लिए सर्वोत्तम अंतिम आश्रय को दर्शाते हैं |
व्यक्ति जो पौधों को जानने के लिए सच्चे मन से किसी भी वानस्पतिक उद्यान में जाता है तो उसे निश्चय ही पौधों की अद्भुत संसार की एक अच्छी समझ प्राप्त होगी | वानस्पतिक उद्यान वनस्पतिज्ञों, बागवानी विशेषज्ञों, पादप संवर्धकों, आनुवंशिक विज्ञानियों, विकासवादी जीवविज्ञानियों, परागाणु विज्ञानियों, संरक्षकों, पर्यावरणीय वैज्ञानिकों एवं अन्य अनुसंधानकर्ताओं को पादप जीवविज्ञान के बहुआयामी पहलूओं पर अध्ययन करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करके एक खुला प्राकृतिक प्रयोगधाला की तरह कार्य करती है |
वर्त्तमान परिपेक्ष्य में, वानस्पतिक उद्यान निम्नलिखित चीजों को बताने के लिए सबसे अच्छा मंच है |
- वानस्पतिक उद्यान पादप जगत के समृद्धता एवं जातियों की समृद्धता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को लोगों को सिखाने के लिए आदर्श स्थान होते हैं |
- यह उन जटिल संबंधो को भी बताता है कि पौधे समय समय पर पर्यावरण के साथ विकसित हुए हैं |
- यह लोगों को यह भी जानने में मदद करता है कि कैसे मानव जाति अपने दैनिक जरूरतों के लिए आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सौंदर्यबोध के दृष्टिकोण से पौधों पर निर्भर हैं |
- पौधों को होनेवाले नुकसानों एवं पौधों के विनाश के परिणामों तथा तत्पश्चात संभावित समाधान ढूँढने के प्रति लोगों को जागरूक करना भी इसका कार्य है |
- लोगों को यह भी सिखाना कि कैसे हमलोग प्राकृतिक संपदा एवं पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश को रोक सकते हैं |
वानस्पतिक उद्यानों की महत्वपूर्ण भूमिकाएं:
- पारंपरिक रूप से, किसी विशिष्ठ जाति को स्पष्ट समझ के लिए जीवंत एवं संरक्षित पादपालय (सूखाया गया सपाट प्रतिरूप जिसे कार्डबोर्ड या मोटे कागज पर उचित लेबल एवं पहचान के साथ मढ़ा होता है ) प्रतिरूपों का तुलनात्मक अध्ययन वानस्पतिक उद्यानों द्वारा किया जा रहा है |
- विश्व भर से महत्वपूर्ण पेशेवर पौधों को लगाना,उगाना एवं इनकी संख्या बढ़ाना तथा नए क्षेत्रों में खेती हेतू निर्गत करने के लिए विभिन्न जांचपरक आधारों पर इनके पर्यावरणीय अनुकूलन क्षमता का अध्ययन करना |
- पौधों के जीवंत डाटाबेस तथा मूल स्थानिक एवं विदेशगत जातियों के आश्रयस्थल की तरह कार्य करने के लिए |
- स्थानिक एवं लुप्तप्राय (ईईटी) जातियों को प्रस्तुत करना एवं संरक्षण करना तथा वन्यस्थलों में पुनर्संयोजन एवं जर्मप्लाज्म का प्रभावशाली संरक्षण हेतु जीवविज्ञान एवं उक्त जातियों के फैलाव पर अनुसंधान कार्य करने के लिए |
- विभिन्न बागवानी संबंधी अनुसंधानों जैसे संकरण, चयन, पर परागण, परिक्षण आदि आयोजित कर किसी क्षेत्र के आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पौधों के उच्च प्रभेदों को विकसित करना |
वर्त्तमान में सम्पूर्ण विश्व भर में लगभग 2000 उद्यान एवं आर्बोरेटा हैं | पिछले 30 वर्षों में संरक्षण आंदोलन की उत्पत्ति के कारण वानस्पतिक उद्यानों ने भी वैज्ञानिक संस्थानों की तरह ही पुनरुत्थान देखा है |
आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वानस्पतिक उद्यान, हावड़ा भारतीय वानस्पतिक उद्यान (आईबीजी) पूर्वतः 'कंपनी बगान',द रॉयल बॉटेनिक गार्डेन (आरबीजी), कोलकाता, के नाम से ज्ञात वर्त्तमान में एजेसी बोस इंडियन बॉटेनिक गार्डेन (एजेसीबीआईबीजी),हावड़ा के नाम से जानी जाने वाली विश्व में प्राकृतिक सौंदर्ययुक्त सबसे अच्छे उद्यानों में से एक है | आईबीजी की वास्तविक इतिहास इंग्लैंड के किव गार्डेन से लगभग मिलती है जो लंदन से कुछ मील दूर थेम्स नदी के तट पर स्थित है | किव गार्डेन की स्थापना के 50 वर्ष बाद हुई | जहाँ आईबीजी हावड़ा, ने राजवंश के लिए वनस्पतिविज्ञान में रूचि लिया वहीं किव गार्डेन की स्थापना आर्थिक और वैज्ञानिक लक्ष्यों के साथ हुई | किव गार्डेन की शुरुआत प्रारंभ में मात्र 15 एकड़ की भूमि के साथ हुआ और समयोपरांत इसका विकास रॉयल बॉटेनिक गार्डेन,किव के प्रथम निदेशक विख्यात वनस्पतिशास्त्री सर विलियम हूकर के हाथों हुआ और अभी यह 288 एकड़ में व्याप्त है | इसके विपरीत द रॉयल बॉटेनिक गार्डेन,कोलकाता हुगली नदी के तट पर कोलकाता से कुछ किलोमीटर दूर स्थित है जिसे 300 एकड़ से भी अधिक विशाल भूभाग में शुरू किया गया था और जो 19वीं सदी के मध्य तक विश्व का सबसे बड़ा एवं प्राचीन बॉटेनिक उद्यानों में से एक था और अभी यह 273 एकड़ में व्याप्त है |
वर्तमान में, यह गार्डेन 273 एकड़ में व्याप्त होने एवं 1377 पादप जातियों के आश्रयस्थल एवं संख्या में 14122 पौधें जिसमे वृक्ष, झाड़ियाँ एवं लत्ते भी शामिल हैं के कारहोने के कारण इसके 25 अनुभाग हैं एवं 24 आपस में जुड़े झील हैं,और सभी झीलें पानी के नियमित प्रवेश एवं निकाषी के लिए नालियों द्वारा गंगा से जुड़े हुए हैं | गार्डेन सीखने एवं उत्सुकता उदबोधन का एक अनोखा स्थान है तथा इसमें अनोखे आकर्षण भी हैं जैसे 'ग्रेट बनयान ट्री', जो की पादप जगत में एक सजीवन्त रहस्य है; विशाल पाम हाउस जिसमें लोडोइसिया मालदिविका (द्विधारी कोकोनट पाम) सहित पामों का समृद्ध संग्रह है, शाखित पाम (हायफेन थेबेका) जिसे मिस्र से लाया गया है; सेंचुरी पाम (कोरिफा मैक्रोपोडा); अमेजन नदी से लायी गयी जाइंट वाटर लिली (विक्टोरिया अमेजनिका); बर्मा मूल से पुष्पीय वृक्षों की रानी (एम्हर्स्टिया नोबिलिस); माउंटेन रोज या वेनेज्युएलन रोज (ब्राउनिया जाति); अफ्रीका मूल का बोबब वृक्ष या कल्पवृक्ष (एडनसोनिया डिजिटाटा); रोसोगोला ट्री (क्रिसोहायलम कैनिटो; कैनन बॉल ट्री (कुरौपिटा गुएनेनसिस); अफ्रीकन सॉसेज ट्री (किजेलिया पिनाटा) एवं मैड ट्री (टेरिगोटा अलाटा वर.इरेगुलरिस )आदि कुछ पादप हैं जो चर्चा योग्य हैं |
कोलकाता में बॉटेनिक गार्डेन स्थापित करने के निर्णय का श्रेय एक जिज्ञासु बागवानिशास्त्री कर्नल रॉबर्ट किड जो सम्मानजनक ईस्ट इंडिया कंपनी के डॉकयार्ड के अधीक्षक एवं बंगाल इन्फैंट्री के फोर्ट विलियम स्थित मिलिट्री बोर्ड के सचिव थे की तीव्र अभिलाषा एवं उसके अथक प्रयास को जाता है | इस समय बंगाल 'ग्रेट बंगाल फेमिन' जैसे संकट एवं इसके परिणामस्वरूप फसलों की असफलता से जूझ रहा था | ईस्ट इंडिया कंपनी सुखाड़ की पुनरावृति को रोकने के लिए उचित एवं प्रभावशाली उपायों की खोज में था | कर्नल कैद ने जनवरी 1786 को लिखी गयी अपने ऐतिहासिक पत्र में उस समय के कार्यवाहक भारतीय जनरल
सर जॉन मैकफरसन को बॉटेनिक गार्डेन की स्थापना से जुड़े लाभों के बारे में अपनी राय दी जिसमें आगे यह भी लिखा गया " यदि समुचित सहयोग किया गया तो दूसरे देशों से लाए जाने वाले फलों एवं खाने की सब्जियों को उगाने में निश्चित सफलता मिल सकती है क्योंकि बंगाल की मिट्टी एवं जलवायु उत्पादन के लिए अनुकूल है ....... इतना ही नहीं बिना असफलता के व्यापार की अभी तक नहीं खोजी जा सकी जंगलों एवं मरुभूमियों में विद्यमान वस्तुओं को भी प्रतिस्थापित किया जा सकता है तथा उन वस्तुओं की खेती को भी बढ़ावा दिया जा सकता है जो ग्रेट ब्रिटेन के उत्पादनकर्ताओं के लिए उपयोगी होगा और इसलिए भारत में निवेश महत्वपूर्ण हो जाता है " आगे वह यह भी लिखता है " मुझे कोई संदेह नहीं की आपके आधिपत्य के प्रभाव एवं दिशा -निर्देश में मात्र कुछ ही वर्षों में न केवल उन सभी चीजों की पूर्ति करने में सक्षम हो जाएंगे जो अभी भारत, चीन एवं अरब से लाने की आवश्यकता पड़ती है बल्कि उनकी खेती भी संभव हो पाएगी जो ग्रेट ब्रिटेन की शक्ति एवं व्यापार को बढ़ावा देगी एवं आपके आधिपत्य की सरकार में राष्ट्रों की सम्पति एवं खुशियों में भी बढ़ोत्तरी होगी |" अविलम्ब किड के प्रस्ताव को कोलकाता में बॉटेनिक गार्डेन की स्थापना के लिए आदेश की मंजूरी इंग्लैंड के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से मिल गयी | गार्डेन का वर्त्तमान भूभाग उस समय 310 एकड़ की थी जो शालीमार में किड की निजी गार्डेन के नीचे अधिग्रहित की गयी |
कर्नल किड गार्डेन का प्रथम अवैतनिक अधीक्षक होकर भी अनेक विदेशी पौधों को लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया | वह 1793 में अपने मृत्यु तक अधीक्षक के पद पर बना रहा | 1795 में उनके द्वारा चयनित स्थल पर उनकी याद में एक स्मारक बनाया गया (यह गार्डेन के लगभग केंद्र में अवस्थित है )| यह संगमरमर से बना एक महत्वपूर्ण पेडस्टल है जिसमें एक सुन्दर संगमरमर से बना कलश है जिसमे "रॉबर्ट किड,मिल. ट्रिब. हॉर्टी. फंडाटोरी, पोसूट. ए.के.एम.डी. सीसीएक्ससीवी" उत्कीर्ण है और जिसे मूर्तिकार बैंक्स द्वारा डिजाइन किया गया है |
मद्रास में कार्यरत कंपनी का वनस्पतिज्ञ, डॉ. विलियम रॉक्सबर्ग को 1793 में प्रथम आधिकारिक अधीक्षक नियुक्त किया गया | रॉक्सबर्ग ही वह पहला व्यक्ति था जिसने गार्डेन में उस समय उगने वाले पौधों का एक सूची प्रस्तुत किया | बाद में इसे 1814 में आदरणीय डॉ. विलियम कैरी द्वारा दो खंडों में "होर्टस बंगालेंसिस " शीर्षक के रूप में प्रकाशित किया गया | भारतीय पौधों पर रॉक्सबर्ग के महत्वपूर्ण कार्य के लिए ही 'फादर ऑफ इंडियन बॉटनी' की उपाधि दी गयी |इस समय तक "यूनाइटेड ब्रदरहुड" के नाम से प्रसिद्ध साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जॉन गेराल्ड कोएनिग द्वारा कर लिया गया जो लीन्यूस का एक विद्यार्थी था और जो भारत में सुव्यवस्थित वानस्पतिक अध्ययन के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता था | विलियम रॉक्सबर्ग की मृत्यु 1815 में एडिनबर्ग में हो गयी | उनकी स्मृति में 1882 में ग्रेट बनयान ट्री के उत्तरी भूभाग में एक स्मारक बनाया गया | उसके बाद, 1813 से 1816 तक एच.टी. कोलब्रूक, सर बुचनान हैमिल्टन, जेम्स हेर एवं थॉमस कैसी जैसे अनेक मार्गदर्शकों ने गार्डेन का कार्यभार संभाला |
1817 में एक कुशल एवं ऊर्जावान वनस्पतिज्ञ नाथानियल वालिस को गार्डेन का अधीक्षक नियुक्त किया गया | वे इंडियन बॉटेनिक गार्डेन के इतिहास में लम्बे समय तक सेवा देनेवाले अधीक्षक थे एवं 1846 तक कार्यालय में पद पर बने रहे | इस समय तक गार्डेन के पूर्वी भाग का टिक पौधरोपण सहित 40 एकड़ भूमि कोलकाता के लॉर्ड बिशप (डॉ. मिडलटन) को एक क्रिश्चन कॉलेज हेतु जो बिशप कॉलेज के नाम से जाना जाता है को दिया गया | यह कॉलेज प्रगति किया और वर्तमान में एक विख्यात संस्थान यानी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी (आईआईएसटी), शिबपुर के रूप में जाना जाता है | 1836 में 2 एकड़ भूमि एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी ऑफ इंडिया को दिया गया जिसकी नींव इसके प्रथम अध्यक्ष आदरणीय डॉ. विलियम कैरी द्वारा रखी गयी थी | यह और 25 एकड़ में विस्तारित हुआ एवं 1872 तक गार्डेन अधिकारियों की सहायता से चलता रहा | 1872 में सोसाइटी गार्डेन को वर्त्तमान स्थल अलीपुर, वायसराय हाउस (बेल्वेडर)के निकट स्थानांतरित गया |डॉ. वालिस की मृत्यु 1854 में हुई; वानस्पतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा यादगार रहेगा एवं विशेषकर पादप प्रतिरूपों के संग्रहों एवं प्रख्यात कैटलॉग जिसे 'वालिश कैटलॉग' के नाम से जाना जाता है इसे सेन्ट्रल नेशनल हर्बेरियम, कोलकाता में रखा गया है | उनके दोस्तों एवं प्रशंसकों ने उनकी याद में वर्त्तमान पाइनटम सं. 1 (बैम्बूसेटम के विपरीत तरफ) के निकट स्मारक बनवाया है | वालिस के बाद अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों जैसे डॉ. हुग फॉल्कनर, डॉ. जी. मैकक्लीलैंड, डॉ. थॉमस थॉमसन, डॉ. थॉमस एंडरसन, श्रीमान सी.बी. क्लार्क आदि ने कार्यालय में योगदान दिया | 1864 में कोलकाता में हुगली नदी से बलशाली तूफान युक्त भीषण चक्रवात आया जिसके परिणामस्वरूप गार्डेन के अधिकांश हिस्सों को जलमग्न कर दिया, कुछ स्थानों में तो जल स्तर लगभग 8 फिट तक बढ़ गया तथा चक्रवात के कारण भीषण तबाही के साथ दो जहाज गार्डेन में घुस गए | अनगिनत झाड़ियों सहित कुल वृक्षों की आधी संख्या नष्ट हो गए | बची हुई संख्या बहुत अधिक विक्षिप्त थी एवं पत्त्ति, पुष्प या फल के अंश ही बचे थे | तीन वर्ष बाद बाद थोड़ी काम तीव्रता लेकिन फिर भी बहुत विध्वंसकारी चक्रवात आया जिसने 750 से भी अधिक जीवित वृक्षों को उखाड़ दिया | थॉमसन एंडरसन अपने सम्पूर्ण शेष अवधि में इन मलबों को हटाने के लिए अथक मेहनत किया एवं 1868 में अपने प्रस्थान के पहले गार्डेन में विधिवत पौधरोपण को गति दिया | डॉ. जॉर्ज किंग जिन्होंने 1871 में अधीक्षक का पदभार लिया गार्डेन का पुनर्निर्माता बन गया (गार्डेन का वर्त्तमान भूभाग उनके द्वारा बनाया गया)| उन्होंने उस समय पदभार लिया जिस समय गार्डेन सर्वाधिक निराशाजनक अवस्था में थी | लगातार आने वाले विनाशकारी चक्रवातों के कारण गार्डेन के अधिकांश क्षेत्र में मोटे घांस एवं आंशिक दलदल में बढ़ोत्तरी हुई | अधिकांश सड़के संकरी थी जो प्रायः बाढ़ में डूबे होते थे एवं मालवाहक वाहनों के लिए अनुपयुक्त थे; एवं झीलें बेढंगे एवं टैंकों में परिवर्तित हो गए |
डॉ. किंग के दृढ़ संकल्प एवं दृढ़ प्रतिज्ञा ने गार्डेन को वर्त्तमान स्वरुप में बदल दिया | सम्पूर्ण मैदान को समतल कर दिया गया है एवं बहुत बड़े भूभाग में आवश्यक मिट्टी कटाई की गई जिससे कृत्रिम झीलों का निर्माण हुआ | इन झीलों को एक दूसरे से भूमिगत पाइपों द्वारा जोड़ा गया एवं एक वाष्प पम्प लगाया गया है जिसके द्वारा गंगा से जल खिंचा जा सके एवं सम्पूर्ण सिस्टम में में जल को उच्च स्तर में रखा जा सके | मालवाहनों एवं लोगों के आवागमन के लिए अनेक चौड़ी सडकों एवं फुटपाथों का निर्माण किया गया | पुरानी शैली पर आधारित संरक्षणालयों (बैम्बू एवं मैट इरेक्शंस)को विशाल,आकर्षक एवं लोहे से बने सक्षम आकृतियों जिस पर उष्ण कटिबंधीय पौधों को उगाने के लिए घांस की पतली परत फैलायी जाती है | मूलयवान पादपालय संग्रहों को उचित तरीके से उस समय के सरकारी वास्तुकला विशेषज्ञ,श्री ई.जे. मार्टिन द्वारा डिजाइन किए गए सुन्दर भवन में रखे जाते हैं | नवीन प्रसारण आश्रयों, यंत्रों एवं गमलों के शेडों को बनाया गया है एवं स्थापना के सदस्यों हेतु सुन्दर निवास स्थलों का निर्माण किया गया है | अंशतः गार्डेन के चारों ओर एक सीमावर्ती दीवार एवं नहर बनाए गए हैं | स्वदेशी एवं विदेशी दोनों प्रकार के पौधों का संग्रह बहुतायत बढ़ चूका है | सड़क एवं स्टीमर द्वारा गार्डेन तक की यातायात सुविधाओं में वृद्धि हुई हैं | इस महान उपलब्धि के लिए डॉ. किंग को महारानी द्वारा 'सर' की उपाधि से सम्मानित किया गया और बाद में उन्हें सर डॉ. जॉर्ज किंग के रूप में जाना गया | वे 1890 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के संस्थापक निदेशक भी रहे हैं |
जॉर्ज किंग के बाद लेफ्टीनेंट कर्नल डेविड प्रैन पद ग्रहण किया एवं 26 वर्षों की गुणवत्तापूर्ण सेवा के बाद 1897 में सेवा निवृत हुआ | वर्ष 1904 में सर डेविड ने भारत छोड़ने के पहले गार्डेन विभाजन संबंधी भौगौलिक योजना तैयार किया जिसके अनुसार भविष्य में पौधारोपण किया जाना था | सर डेविड प्रैन की योजना में थोड़ी बदलाव कर उसके बाद के व्यक्तियों द्वारा अनवरत अनुपालन किया गया |
सर डेविड के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल ए.टी. गेज 1906 में गार्डेन का अधीक्षक बना | रॉयल बॉटेनिक गार्डेन,कलकत्ता में उगाई गयी पुष्पोद्भिदी अऔषधीय पौधों का कैटलॉग लेफ्टिनेंट कर्नल ए.टी. गेज के समय तैयार किया गया जिसे दूसरे संस्थानों के साथ पादप सामाग्रियों के आदान -प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया | कर्नल ए.टी. गेज के बाद 1923 में श्री काल्डर आया | भारत से अवकाश पर श्री काल्डर के अनुपस्थिति के दौरान डॉ. जे.एम. कोवन ने 12 जुलाई 1926 से 20 नवंबर 1927 तक अधीक्षक के रूप में कार्य किया |
1937 में प्रथम भारतीय, के.पी. बिश्वास गार्डेन के अधीक्षक का पद ग्रहण किया एवं 1955 तक पद पर बना रहा | वर्त्तमान नाम 'एजेसी बोस इंडियन बॉटेनिक गार्डेन' 24 जून, 2009 से अस्तित्व में आया |
गार्डेन के अभूतपर्व जातियों का परिचय: हावड़ा स्थित इंडियन बॉटेनिक गार्डेन निश्चित रूप से विश्व के विभिन्न भागों के पेशेवर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अनेक पौधों के समावेशन, गुणन एवं वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है |कुछ विशेष पौधों के समावेशन ने जन कल्याण एवं देश के आर्थिक विकास को प्रत्यक्ष प्रभावित किया है |
चाय:
चाय के कप बिना हमारे लिए एक भी दिन की कल्पना करना कठिन है | भारत में चाय की खेती एवं मद्यकरण का पारम्परिक चिकित्सा पद्यति एवं इसके सेवन में अनुप्रयोगों का एक लम्बा इतिहास रहा है | चाय का चीन से भारत में समावेशन की सही तिथि स्पष्ट ज्ञात नहीं है | यह ज्ञात है की चाय का इंडियन बॉटेनिक गार्डेन, हावड़ा में पहली बार समावेशन गुआंझू से रॉक्सबर्ग के काल में हुआ | ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक चाय समिति का निर्माण किया जिसमे डॉ. एन.वालिस, जी.जे. गॉर्डन एवं डब्लू ग्रांट शामिल थे | हालांकि चीनी चाय लोगों में बहुत अधिक रूचि उत्पन्न नहीं कर सका |
1823 में जब रॉबर्ट ब्रुस (एक सैन्य अधिकारी) ब्रह्मपुत्र होते हुए असम की यात्रा कर रहे थे तभी दिहांग नदी के निकट 'सिंगफो' एवं 'खाम्ति' जनजातियों से मुलाकात हुई और उन्होंने देखा कि वे स्थानीय चाय की झाड़ियों से चाय तैयार कर सेवन करते हैं | उसके छोटे भाई एलेक्जेंडर ने अपने भाई के खोज का अनुसरण करते हुए उस इलाके से इस पौधे के कुछ सीडलिंग्स को बाद में लाया एवं इंडियन बॉटेनिक गार्डेन, हावड़ा में समावेशित किया | इसके बाद, 1834 में फ्रांसिस जेनकिन्स ने इंडियन बॉटेनिक गार्डेन, हावड़ा में विस्तृत पैमाने पर चाय की खेती का प्रयास किया एवं कुछ प्रतिरूपों को डॉ. वालिस के पास भेजा जिसने इसे कैमेलिया थेइफेरा के रूप में पहचान किया,जो चाय का स्रोत है | इस प्रकार गार्डेन ने भारत में चाय की खेती का नींव रखा |
आज भारत विश्व में चाय का सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है,हालांकि चाय का 70% भारत में ही उपभोग किया जाता है | असम एवं दार्जिलिंग जैसे विश्व विख्यात अनेक चाय मुख्यतः भारत में ही उगाए जाते हैं | भारतीय चाय उद्योग अनेक वैश्विक चाय ब्रांड के रूप में विकसित हुआ है एवं विश्व में सर्वाधिक तकनीक युक्त चाय उद्योगों के रूप में उभरा है | भारत में चाय उत्पादन, प्रमाणन, अन्वेषण एवं चाय के व्यापार संबंधी अन्य सभी पहलूओं को भारतीय चाय परिषद द्वारा नियंत्रित किया जाता है |
सिनकोना:
सिनकोना वृक्ष के औषधीय गुणों की खोज 'क्यूचुआ' द्वारा किया गया जो पेरू एवं बोलिविया के लोग थे एवं उन्हीं लोगो के द्वारा निम्न तापमान के कारण मांसपेशियों में होने वाले सिकुड़न एवं कम्पन को रोकने के लिए खेती की जाती थी | जेस्यूइट ब्रदर अगोस्टीनो सलअम्ब्रिनो (1561-1642),प्रशिक्षण से औषधी बनाने वाला लिमा निवासी ने क्युएचुआ को कंपकपाहट से बचने के लिए क्यूनिन युक्त सिनकोना के वृक्ष के छाल का प्रयोग करते हुए देखा | जबकि मलेरिया के इलाज में ठंड से कंपकपी का नियंत्रण इसका प्रभाव से संबंधी नहीं था फिर भी मलेरिया के इलाज का यही सही औषधि था | थॉमस एंडरसन जब 1861 में इंडियन बॉटेनिक गार्डेन का अधीक्षक बना उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में मलेरिया महामारी के प्रकोप की एक डरावनी तस्वीर व्याप्त थी, एवं इस बीमारी के कारण हजारों लोग उस समय वर्ष में मर रहे थे | एंडरसन ने भारत में सिनकोना पौधों के समावेशन (लाने) में मुख्य भूमिका निभाया | उसने 1861 में किव से सिनकोना के कई जातियों को लाया (यह पौधा मूलतः दक्षिण अमेरिका से था) एवं ट्रायल खेती के लिए इंडियन बॉटेनिक गार्डेन,हावड़ा में इसका सीडलिंग उगाया | बाद में एंडरसन ने मंगपु एवं दार्जिलिंग की पहाड़ियों में सिनकोना की खेती का प्रारम्भ किया | अपने खराब स्वास्थ्य के कारण एंडरसन ने कार्य पूरा नहीं कर सका और बाद में यह कार्य अन्य अधीक्षकों जैसे सी.बी. क्लार्क एवं जॉर्ज किंग द्वारा आगे बढ़ाया गया | वे मांगपू के सिनकोना पौधरोपण के अधीक्षक भी रहें | मंगपु में उगाए गए सिनकोना सकिरुबरा की जांच प्रभावशाली तरीके से की गयी एवं चिकित्सकों द्वारा मान्यता दिया गया तथा बाज़ार में मलेरिया के इलाज हेतु प्रभावकारी दवा के रूप में निर्गत किया गया | इस तरह से, इंडियन बॉटेनिक गार्डेन ने मलेरिया के इलाज हेतु प्रभावकारी दवा प्रदान कर लाखों की जान बचायी |
रबड़:
हिविया ब्रासिलिएन्सिस, पारा रबड़ वृक्ष प्रारम्भ में केवल अमेजन वर्षावन में ही उगाया जाता था | इस वृक्ष का नाम ब्राजील की दूसरी सबसे बड़ी राज्य पारा से लिया गया है,जिसकी राजधानी बेलम है | इन वृक्षों का प्रयोग मूलवासियों द्वारा रबड़ प्राप्त करने में किया जाता था जो इसके भौगौलिक वितरण के क्षेत्र में रहते थे | बढ़ती हुई मांग एवं 1839 में वल्कनीकरण प्रक्रिया की खोज ने उस क्षेत्र में रबड़ की खेती में गति आई जिससे बेलम एवं मनौस महानगरों को समृद्ध किया | सर जे.डी.हूकर, उस समय के रॉयल बॉटेनिक गार्डेन किव के निदेशक द्वारा दिए गए हिविया ब्रासिलिएन्सिस (पारा रबड़) को 1873 में सर जॉर्ज किंग ने खेती के लिए इंडियन बॉटेनिक गार्डेन,कोलकाता में लाया | उसने इन पौधों को कोलकाता में स्थापित करने का पुरजोर कोशिश किया | हालांकि उसे प्रायः निराशा का सामना करना पड़ा क्योंकि कोलकाता की जलवायु रबड़ की खेती के लिए उपयुक्त नहीं थी | बाद में उन पौधों को ब्रिटिश साम्राज्य के उपयुक्त जलवायु वाले अन्य क्षेत्रों जैसे बर्मा, मलाया, दक्षिण भारत एवं सिलोन में भेज दिया गया | अभी हमलोग देख सकते हैं कि रबड़ इन क्षेत्रों में मुख्य व्यावसायिक फसल है |
महोगनी:
इंडियन बॉटेनिक गार्डेन का प्रसिद्ध महोगनी परिसर आगंतुकों से परिचित है | गार्डेन के शुरू होने के कुछ वर्षों बाद 1795 में इंडियन बॉटेनिक गार्डेन, हावड़ा में वेस्ट इंडीज से समावेशित किया गया, यह उच्च गुणवत्तापूर्ण टिम्बर देने वाली महोगनी के सफल समावेशन का एक गवाह है | उस समय के किव बॉटेनिक गार्डेन,इंग्लैंड के निदेशक सर जे.डी. हूकर, ने महोगनी के कई जातियों को इंडियन बॉटेनिक गार्डेन, हावड़ा में स्थापित करने के लिए आपूर्ति किया | यहाँ बड़े पैमाने पर महोगनी का गुणन किया गया एवं भारत के विभिन्न भागों में वितरित किया गया | आज भारत के वन क्षेत्रों में पाए जाने वाले उच्च गुणवत्तापूर्ण टिम्बरों में से एक है |
व्यावसायिक समावेशन एवं गुणन:
गार्डेन ने बहुत बड़ी संख्या में आर्थिक एवं मसालों की जातियों जैसे इलायची, सिनकोना, कॉफी, कॉटन, इंडिगो, नटमेग, पिपर, लौंग, ईख, आलू, सागो, टिक आदि के अनुकूल जलवायुकरण एवं वितरण के लिए प्लेटफॉर्म की तरह कार्य किया है | एवं चारा, पशु आहार, तेल,फल, टिंबर एवं सजावटी पौधों का पहली बार समावेशन इसी ऐतिहासिक गार्डेन में किया गया | अधिकांश समावेशित जातियों का गुणन गार्डेन में ही हुई एवं इन्हे व्यावसायिक खेती के लिए देश के विभिन्न भागों में वितरित किया गया | इस गार्डेन से कुछ अन्य रोचक पौधों को भी समावेशित किया गया जैसे 1826 में नथानियल वालिस द्वारा बर्मा से अम्हेर्स्टिया नोबिलिस (पुष्पीय वृक्षों की रानी); डब्लू. हैमिल्टन द्वारा 1803 में अलामंदा एसपी; डब्लू. हैमिल्टन द्वारा 1803 में बौगेनबोलिया एसपी.;सी. स्मिथ द्वारा 1798 में गार्डेन क्रोटन ; 1798 में ऑस्ट्रेलियन पाइन ; डब्लू. हैमिल्टन द्वारा 1795 में क्रेसेंटिया क्युजीटी (कलाबेश वृक्ष); सर जॉर्ज किंग द्वारा 1874 में लोडोइसिया मालदीविका (डबल कोकोनट); 1797 में पैशन फ्लावर; विलियम रॉक्सबर्ग द्वारा 1794 में चायनीज रोज; सर जॉर्ज किंग द्वारा 1873 में विक्टोरिया अमेजनिका (जाइंट वाटर लिली) | पूर्ववर्ती उदाहरणों में कुछ ही चर्चा किए गए हैं |
परिपेक्ष्य में बदलाव:
ऐतिहासिक अर्थ समिट (यूनाइटेड नेशंस कांफ्रेंस ऑन इन्वायर्नमेंट एंड डेवलपमेंट- यूएनसीएडी) का आयोजन 3 जून से 14 जून 1992 तक ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया एवं इसके बाद वार्तालाप एवं प्रतिभागी देशों के हस्ताक्षर के लिए कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी (सीबीडी) के खुलने से वैश्विक जैवविविधता के संरक्षण हेतु उपायों को पुनर्परिभाषित करने की नई दिशा की शुरुआत हुई | सीबीडी विशेषकर विश्व के हजारों संकटग्रस्त जातियों के संरक्षण की आवश्यकता एवं लुप्तप्राय दुर्लभ, संकटग्रस्त पादप जातियों को उनके प्राकृतिक आवासों से अलग संरक्षण में बॉटेनिक गार्डेन्स (एक्स-सीटू संरक्षण) किस तरह की भूमिका निभा सकती है इस बात पर जोर डालती है | कन्वेंसन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी (सीबीडी), सामान्यतः बायोडायवर्सिटी कन्वेंसन के नाम से ज्ञात एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी बन्धनयुक्त ट्रीटी है | पूर्व के संरक्षण प्रयासों का लक्ष्य किसी विशेष जाति एवं आवासों की सुरक्षा से था किन्तु कन्वेंशन ने पहचाना की पारिस्थितिकी तंत्रों , जातियों एवं वंशों का प्रयोग मानव कल्याण के लिए किया जाना चाहिए | हालांकि, यह इस तरह से किया जाना चाहिए एवं इस दर से किया जाना चाहिए कि जैव विविधता का दीर्घकालिक पतन की ओर अग्रसर न हो सके | कन्वेंसन ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क़ानून में जाना कि जैव विविधता का संरक्षण "मानव जाति का सामान्य चिंता है" एवं विकास प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है | इस समझौता के अंतर्गत सभी पारिस्थितिकी तंत्र, जाति एवं जेनेटिक संसाधन आते हैं |